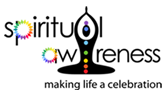भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।।4।।
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ।।5।।
श्री भगवान बोले- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी- इस प्रकार यह आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात् मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो! इससे दूसरी को, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् धारण किया जाता है, वह मेरी जीवरूपा परा अर्थात् चेतन प्रकृति जान।
व्याख्या (Interpretation Of Sloka 4-5 | Bhagavad Gita Chapter 7)-
परमात्मा सबके कारण हैं। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं, उसका नाम ‘‘अपरा प्रकृति’’ है और अपना अंश जो जीव है, उसको भगवान् परा प्रकृति कहते हैं। ‘‘अपरा प्रकृति’’ निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा ‘‘परा प्रकृति’’ श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है।
‘‘ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखरासी’’
यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम ‘‘प्रकृति’’ है। परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होेने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ सम्बन्ध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है।
यदि यह परा प्रकृति (जीव) अपरा प्रकृति से (शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार) विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाये, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने अर्थात् अपरा प्रकृति से सर्वथा सम्बन्ध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाये। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से सम्बन्ध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वह प्रेम अनन्त, अगाध, असीम, आनन्द स्वरूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असंख्य रूप का अनुभव होने से ज्ञात-ज्ञातव्य (जो जानना था सो जान लिया) हो जाती है और अपरा प्रकृति (शरीर, मन, बुद्धि,अहंकार) को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृत-कृत्य हो जाती है। यही मानव-जीवन की पूर्णता है, सफलता है।
जीव भूतां– वास्तव में यह जीवरूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात् परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ सम्बन्ध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह सम्बन्ध जोड़ता है- अपने सुख के लिए, मान-प्रतिष्ठा के लिए। यही सुख, मान-प्रतिष्ठा इसके जन्म-मरण रूप महान् दुःख का खास कारण हो जाते हैं।
वास्तव में यह जगत् जगतरूप नहीं है, प्रत्युत भगवान् का ही स्वरूप है- ‘‘वासुदेवः सर्वम्’’। (गीता -7/19, 9/19) केवल इस परा प्रकृति-जीव ने इसको जगतरूप से धारण कर रखा है अर्थात् जीव इस संसार की स्वतन्त्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया, इसी से जीव का बन्धन हुआ है। यदि जीव संसार की स्वतन्त्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवद्-स्वरूप ही माने तो उसका जन्म-मरण रूप बन्धन मिट जायेगा।
जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थाई, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमानजन्य सुख होता है और भोगों से संयोगजन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत् को जगतरूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत् को भगवद्स्वरूप से नहीं देख सकता।
नदी के किनारे खड़े एक सन्त से किसी ने कहा कि- देखिए महाराज यह नदी का जल बह रहा है। सन्त ने उससे कहा कि- देखो भाई! नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथ मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न ये नदी रहेगी, न ये पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेगा।
ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है अर्थात् प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दीखने वाला ये सारा जगत् प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। परन्तु जीव ने इसको भावरूप से अर्थात् ‘‘है’’ रूप से धारण (स्वीकार) कर रखा है जिससे यह जन्मता-मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ सम्बन्ध न जोड़े, इससे विमुख हो जाये अर्थात् भावरूप से इसको सत्ता न दे तो जगत् सतरूप से दीख ही नहीं सकता।
भक्तियोग में ‘‘मैं केवल भगवान् का हूँ और केवल भगवान् ही मेरे हैं। तथा मैं शरीर-संसार का नहीं हूँ और शरीर-संसार मेरे नहीं हैं-’’ ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवद् परायण हो जाता है। जिससे संसार का सम्बन्ध स्वतः टूट जाता है और अहमता की निवृत्ति हो जाती है।
परिशिष्ट भाव –
जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है अर्थात् ‘‘अहम्’’ के साथ एक होकर अपने को ‘‘मैं हूँ’’ ऐसा मान लेता है, तब वह जीवरूप बनी हुई ‘‘परा प्रकृति’’ कहलाता है। ‘‘अहम्’’ (मैं) से इधर ‘‘जगत्’’ (अपरा प्रकृति) है और उधर ‘‘परमात्मा’’ हैं। परन्तु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके, प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगतरूप से धारण कर लेता है और जन्म-मरण रूप बन्धन में पड़ जाता है।
जगत् की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, बाँधने वाला जगत् तो जीव ने ही बना रखा है। जीव जगत् को धारण करता है- इसी से सुख-दुःख होते हैं, बन्धन होता है, चैरासी लाख योनियाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, देवता आदि योनियाँ तथा नरकों की प्राप्ति होती है।
सत, रज और तम- ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परन्तु इनका संग करने से जीव उर्ध्वगति, मध्यगति, अथवा अधोगति में जाता है। (गीता 13/21) गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं करती। सम्बन्ध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इन्द्रियाँ करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही सम्बन्ध करता है इसलिए सुखी-दुःखी हो रहा है, जन्म-मरण में जा रहा है। जीव स्वतन्त्र है, क्योंकि यह ‘‘परा’’ अर्थात् उत्कृष्ट प्रकृति है। ‘‘अपरा’’ प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती, क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे सम्बन्ध जोड़कर उसका सदुपयोग-दुरूपयोग करके जीव ऊँच-नीच योनियों में जाता है, भटकता है। तात्पर्य है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत् के साथ सम्बन्ध जोड़कर परिवर्तनशील जगतरूप हो जाता है। (गीता 7/13)
उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरणा होती ही नहीं।
जो हमसे सर्वथा अलग है, उस जगत् अर्थात् शरीर- इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि-अहम् के साथ अपनी एकता मान ली- यही जगत् को धारण करना है। वास्तव में जगत् हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनायें सदा के लिये मिट जाती। हम निर्मम, निर्भय, निश्चिन्त, निष्काम हो जाते। परन्तु जगत् हमें ऐसी चीज नहीं दे सकता, जो हमारी हो अर्थात् जो हमसे कभी बिछुड़े नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है, वह जगत् के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, प्रत्युत जगत् के सम्बन्ध-विच्छेद से प्राप्त हो सकती है। हमारी वस्तु है- “परमात्मा”। हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके –(गीता 15/7)
उसकी प्राप्ति का उपाय (कर्मयोग) की दृष्टि से यह है कि जगत् से मिली हुई वस्तुओं (शरीर आदि) को जगत् की ही सेवा में लगा दें और बदले में उससे कुछ भी आशा (फलेच्छा) न रखें। उससे कोई सम्बन्ध न जोड़ें, न क्रिया के साथ, न पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा, किसी को दुःख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुःख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती।अपने आप होने वाली क्रिया का (जैसे’- भोजन का पचना) अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है।
वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं- ‘‘नासतो विद्यते भावः’’। उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे- रूपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं, उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं, जब दोषों को स्वीकार करते हैं। संसार के सब सुख दोषजनित हैं। दोषों को स्वीकार करने से ही सुख दीखता है। कामरूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है, लोभरूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है, मोह रूप दोष के कारण ही कुटुम्ब-परिवार में आकर्षण होता है आदि। परन्तु दोषों को न जानने के कारण हमें इस बात का पता ही नहीं लगता कि हम ही उनको (अपरा प्रकृति को) सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते ही नहीं और गुण दीखते नहीं।
अनन्त ब्रह्माण्डों में तीन लोक, चौदह भुवन, जड़-चेतन, स्थावर-जंगम, थलचर-जलचर-नभचर, जरायुज-अडंज-स्वेदज-उद्भिज, सात्विक-राजस-तामस, मनुष्य-देवता-पितर-गन्धर्व-पशु-पक्षी, कीट-पतंग, भूत-प्रेत-पिशाच, ब्रहम-राक्षस आदि। जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें परा और अपरा- इन दो प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम् के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब ‘‘अपरा’’ है। परन्तु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है वह ‘‘परा’’ है। ‘‘परा’’ और ‘‘अपरा’’ दोनों ही भगवान् की शक्तियाँ होने से भगवान् से अभिन्न अर्थात् भगवद् स्वरूप ही हैं। अतः अनन्त ब्रह्माण्डों के भीतर तथा बाहर और अनन्त ब्रह्माण्डों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचिन् मात्र भी कुछ नहीं है- वासुदेवः सर्वम् -(गीता 7/19, 9/19)।
संसार के सभी दर्शन मत-मतान्तर आचार्यों को लेकर हैं, पर ‘‘वासुदेवः सर्वम्’’ किसी आचार्य का दर्शन, मत नहीं है। प्रत्युत साक्षात् भगवान का अटल सिद्धान्त है, जिसके अन्तर्गत सभी दर्शन, मत-मतान्तर आ जाते हैं।
‘‘अपरा’’ (जगत्) भगवान् का है, पर उसको शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम् अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बन्धन में पड़ा है। यदि साधक को जगत् दिखता है तो उसको निष्कामभावपूर्वक जगत् की सेवा करनी चाहिए। जगत् को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बन्धन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है, वह सब जगत् का है और जगत् के लिए है। अतः जगत् की वस्तु को जगत् की सेवा में लगाने से जगत्, जगतरूप से नहीं दीखेगा, प्रत्युत भगवद्स्वरूप दीखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत् को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अन्तिम तत्त्व‘‘वासुदेवः सर्वम्’’ का अनुभव कर सकता है।
संकलित – श्रीमद् भगवद् गीता।
साधक संजीवनी- श्रीस्वामी रामसुखदासजी।