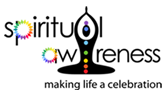येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता: ।।28।।
श्री भगवान बोले- परन्तु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेष जनित द्वन्द्वरूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मेरा भजन करते हैं।
व्याख्या (Interpretation Of Sloka 28 | Bhagavad Gita Chapter 7)
जिन मनुष्यों ने “अपने को तो भगवद्प्राप्ति ही करनी है”- इस उद्देश्य को पहचान लिया है अर्थात् जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है- ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य-कर्मा हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दानादि क्रियायें बाहर से होती हैं।
“अन्तगतं पापं”- कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि “मेरे को तो सिर्फ भगवान की तरफ ही चलना है” तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई; क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। सन्तों ने कहा है कि डेढ़ ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण-दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सदगुण-सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अन्त हो जाता है।
दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान हैं, वे पुण्यकर्मा हैं; क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जायेगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं (श्रीमद्भागवत् – 11/5/42)।
तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि ‘‘अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूँगा’’ तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं।
पुण्यकर्मा लोग द्वन्द्वरूप मोह से रहित होकर और दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वन्द्व कई तरह का होता है। जैसे-
- भगवान में लगें या संसार में लगें? क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है।
- वैष्णव, शैव एवं अन्य कई सम्प्रदायों में से किस सम्प्रदाय में चलें?
- परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत-अद्वैत, सगुण-साकार, निर्गुण-निराकार आदि कई तरह के सिद्धांत हैं, इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें ?
- परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति-योग, ज्ञान-योग, कर्म-योग, ध्यान-योग, हठ-योग आदि कई मार्ग हैं, इनमें से किस मार्ग पर चलें?
- संसार में होने वाले अनुकूल-प्रतिकूल, हर्ष-शोक, ठीक-बेठीक, सुख-दुख, राग-द्वेष आदि सभी द्वन्द्व हैं।
उपर्युक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वन्द्वरूप मोह से युक्त हुये मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं।
मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक-सांसारिक सभी द्वन्द्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी-अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा-विश्वास के अनुसार अपने-अपने इष्ट को सगुण मानें, साकार मानें, निर्गुण मानें, निराकार मानें, द्विभुज मानें, चतुर्भुज मानें अथवा सहस्रभुज आदि कैसे ही मानें, पर संसार की विमुखता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियाँ भिन्न-भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी-बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा-विश्वास होता है, उसके लिये वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निन्दा करना, नीचा मानना दोष है। जब तक मन में साधन-विषयक द्वन्द्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्ररूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति एवं निष्ठा का ही करे तो इससे साधन-विषयक द्वन्द्व मिट जाता है।
मनुष्य की यह प्रकृति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है, तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य-जन्म की सफलता इसी में है। परन्तु जब वह व्यवहार में आता है, तब वह ऐसा सोचता है कि ‘‘साधन-भजन’’ से क्या होगा? सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बेैठे हैं, चीज-वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा? अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन-स्मरण का नित्य-नियम समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है, उतनी भजन-स्मरण, नित्य-नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं।
भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ-हानि कुछ भी हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है, वह आँख मीचते ही कुछ नहीं है और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा? ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर-निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वन्द्व-मोह से छूटे हुए हैं।
“दृढ़व्रता”- कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। भगवान हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजें ‘‘हमें कहीं भी रखें और कैसे भी रखें’’- इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है- ऐसे निश्चय से वे दृढ़व्रती हो जाते हैं। उनके हृदय में यह होता है कि ‘‘भगवान हैं’’, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो भगवान से मतलब है। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि ‘‘हमें संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है।’’
उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किन्तु उनकी मान्यता में संसार निरन्तर नष्ट हो रहा है, निरन्तर अभाव में जा रहा है और सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में भावरूप से एक परमात्मा ही हैं ऐसा मानकर वे दृढ़ व्रती होकर भजन करते हैं। जैसे- पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है।
विशेष बात
मनुष्य को ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थितिरूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हों, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात् भगवान का अंश है। पाप तो प्रतिकूल परिस्थिति देकर नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता है तो (गीता 9/30) ‘‘दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है’’– यह कहना बनता नहीं। पापों के कारण अगर भजन-ध्यान में बाधा लग जाये तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप-पुण्य से मिलकर ही मनुष्य-शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो द्रढ़व्रती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अन्त हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है। अतः जो परिस्थियाँ शरीर तक रहने वाली हैं, वे भजन में बाधा पहुँचायें- ऐसा कभी सम्भव ही नहीं है।
सन्तों की वाणी और सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती हैे- ये दोनों ही केवल साधन-सामग्री हैं। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना- यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थियाँ साधन-सामग्री हो जायेंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फँसने की सम्भावना भी रहती है। परन्तु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से सन्तजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आये हैं।
परिशिष्ट भाव
भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है-
“सन्मुख होए जीव मोहि जबहिं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहिं।।” ( मानस, सुन्दर 44/1)
परन्तु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है । जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात् जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गए हैं, वे राग-द्वेष, हर्ष-शोक, सुख-दुख आदि द्वन्द्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं।
राग-द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं जब तक एक वस्तु में राग रहता है, तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है; क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग-द्वेष रहते हैं, तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सम्बन्ध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, उतने अंश में भगवान से विमुखता रहती है।
“दृढ़व्रता”- ढीली प्रकृति वाला अर्थात् शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत् (संसारी भाव) का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया- इस प्रकार बार-बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत् के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत् का त्याग कर नहीं पाता। अगर वह असत् का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको पकड़ लेता है, उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले, उस पर दृढ़ रहे। छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ (पक्का) रहे तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत् का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जायेगी।
संकलित – श्रीमद् भगवद् गीता।
साधक संजीवनी- श्रीस्वामी रामसुखदासजी।