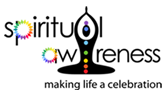जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्रा तद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ।।29।।
श्री भगवान बोले- जो पुरुष मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को सम्पूर्ण अध्यात्म को, सम्पूर्ण कर्म को जानते हैं।
व्याख्या (Interpretation Of Sloka 29 | Bhagavad Gita Chapter 7)
यहाँ जरा (वृद्धावस्था) और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी ही, पर ये दोनों अवस्थायें उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। यहाँ ‘‘जरा मरण मोक्षाय’’ कहने का तात्पर्य जरा-मृत्यु आदि शरीर के विकारों से सम्बन्ध विच्छेद होने में है।
जो जीवन-मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं वे यह जानते हैं कि बुढ़ापा और मृत्यु शरीर के होते हैं। मुझ आत्मा के नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ उनका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद रहता है। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य (मैं यह शरीर हूँ) मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर ‘‘मैं वृद्ध हो गया’’ और शरीर के मरने को लेकर ‘‘मैं मर जाऊँगा’’- ऐसा मानता है। यह मान्यता ‘‘ शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है’’ इसी पर टिकी हुई है।
13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है- जन्म-मृत्यु, जरा और व्याधि में दुःखरूप दोषों को देखना- इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के साथ ‘‘मैं’’ और ‘‘मेरापन’’ का सम्बन्ध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरा-पन से मुक्त हो जायेगा, तब वह जरा-मरण आदि से भी मुक्त हो जायेगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ सम्बन्ध ही वास्तव में जन्म-मरण का कारण है (गीता- 13/21)। वास्तव में हमारा शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं है, जब ऐसा जानते हैं; तभी सम्बन्ध मिटता है। मिटता वही है, जो वास्तव में नहीं होता।
यहाँ ‘‘मामाश्रित्य यतन्ति ये’’ पदों में यह कहा है कि भगवान का आश्रय भी लेना है और यत्न भी करना है- इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि ‘मैंने ऐसा कर लिया, जिससे ऐसा हो गया’’ और अगर स्वयं यत्न न करके ‘‘भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जायेगा’’ ऐसा मानता है तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताईं कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने।
जो नित्य-निरन्तर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर-संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थाई मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थाई मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवद्प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर-संसार को स्थाई न माने और उसको महत्त्व न दे तो भगवद्प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को अर्थात् शरीर-संसार की स्वतन्त्र सत्ता को और महत्ता को विचारपूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परन्तु जो भगवान् का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृृपा से ही साधन-भजन हो रहा है भगवान की कृृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं।
जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने-अपने साधन के अनुसार भगवद्स्वरूप का बोध (मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ एवं शरीर से अलगाव) तो हो जाता है, पर भगवान के समग्ररूप का बोध उनको नहीं होता।
जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान् के समग्ररूप का बोध होकर भगवद्प्रेम की प्राप्ति हो जाती है- यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने अपने आश्रित होने के लिए कहा है।
इस तरह से यत्न (साधन) करने पर वह मेरे स्वरूप को अर्थात् जो निर्गुण-निराकार है, जो मन-बुद्धि-इन्द्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्षरूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानन्दघन ब्रह्म्म को जान जाते हैं (भगवान का आश्रय लेकर)।
उस परमात्मा की सत्ता प्राणिमात्र में स्वतः सिद्ध है। कारण कि वह परमात्मा सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दीखता है? उत्तर है जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है- ऐसे शरीर-संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली, इसी से नित्य प्राप्त परमात्मतत्व अप्राप्त दीख रहा है (संसार की ओर मुख तो भगवान से विमुख)।
सम्पूर्ण जीव तत्त्व से क्या हैं? इस बात को जानना सम्पूर्ण अध्यात्म को जानना है। 15वें अध्याय के 10 वें श्लोक में कहा है कि ‘‘जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को मूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञानचक्षु वाले जानते हैं।’’ आत्मा शरीर से अलग है- इसको तत्त्व से जान जाते हैं अर्थात् अनुभव कर लेते हैं।
सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्त्तव्य और फलासक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्यमात्र को देशकाल, परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्त्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्त्तव्य और फलासक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बाँधने वाला नहीं होता अर्थात् वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है।
जो अनन्य भाव से केवल भगवान् का आश्रय लेता है, उसका प्राकृति क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि यह सब क्रियायें और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान हैं अर्थात् क्रियाओं का आरम्भ और अन्त होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। अतः कर्मों के साथ मेरा किंचिन मात्र भी सम्बन्ध नहीं है- यह भी अखिल कर्म को जानना है।
तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्त्व को जान जाते हैं अर्थात् भगवान ने जैसे कहा है कि ‘‘यह सम्पूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है’’ (गीता 7/7) और ‘‘सब कुछ वासुदेव ही है’’(गीता 7/19), ऐसे ही वे भगवान् के समग्ररूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म- ये सभी भगवद्-स्वरूप ही हैं, भगवान् के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है।
संकलित – श्रीमद् भगवद् गीता।
साधक संजीवनी- श्रीस्वामी रामसुखदासजी।