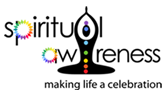यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य:।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ।।15।।
श्री भगवान् बोले – जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष (जलन), भय और उद्वेगादि से रहित है- वह भक्त मुझको प्रिय है।
व्याख्या (Interpretation Of Sloka 15 | Bhagavad Gita Chapter 12)-
भक्त सब प्राणियों में भगवान् को देखता है, इसलिए किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता।
भक्त की दृष्टि में मन-वाणी और शरीर से होने वाली सम्पूर्ण क्रियायें एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं।-(गीता 6/31) ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुँचा सकता है, फिर भी भक्तों के चरित्र में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा, आदर, सत्कार, तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनके सौम्य स्वभाव से कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं।
भर्तहरि जी कहते हैं- हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और सन्तोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं (किसी को कुछ नहीं कहते), परन्तु व्याध, मछुए, और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं।
वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिन्तन और संग-दर्शन-स्पर्श-वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए। ऐसा होने में भक्तों का उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है।
‘‘उमा सन्त कई ईहई बढ़ाई। मन्द करत जो करई भलाई।।” (मानस – 5/41/4)
मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है, जब उसकी कामना मान्यता, साधना, धारण आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा निष्काम होता है इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता।
“हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो” – सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वथा रहित होता है। पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित (प्रसन्नता शून्य) होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य, एकरस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक, नाशवान तथा घटने-बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवान को देखने के कारण वह सदा ही प्रसन्न रहता है।
किसी के उत्कर्ष (उन्नति) को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों की सुख-सुविधा, धन-विधा, महिमा, आदर-सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अन्तःकरण में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है। यह अमर्ष कहलाता है।
अगर साधक के हृदय में दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर अमर्ष का भाव पैदा हो जाए, तो वो उसे पतन की ओर ले जायेगा। और यदि ऐसा भाव उत्पन्न हो कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो तो यह भाव उसके साधन में सहायक होगा।
भय- इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। भय दो कारणों से होता है।
- बाहरी कारणों से- जैसे- सिंह, साँप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचाने की आशंका से होने वाला भय।
- भीतरी कारणों से- जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय।
सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मृत्यु का भय बना रहता है। साधक को भी प्रायः सत्संग, भजन, ध्यानादि साधनों से छूट जाने का भय रहता है। उसको यह भी भय होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा? साधारण मनुष्यों को बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर (जड़ता) के आश्रय से ही पैदा होते हैं। भक्त सर्वथा भगवान् के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवान के चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। सिद्ध भक्त तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही देखता है, फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है।
“उद्वेग”- मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। कई कारणों से मनुष्य को उद्वेग हो सकता है जैसे- बार-बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, कार्य का इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकम्प, बाढ़, आदि दुःखदाई घटनाओं का होना। अपनी कामना, मान्यता, सिद्धान्त अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि। भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है।
भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फलरूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल- प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपा पूर्ण विधान ही देखता है और निरन्तर आनन्द में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है।
“मुक्तः” – पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। अन्तःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतया मन-बुद्धि न लगने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परन्तु भक्त की दृष्टि में एक भगवान् के सिवाय अन्य किसी की स्वतन्त्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण-सदाचार रहते हैं।
भक्त को तो प्रायः इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। यदि कोई गुण दीखता भी है तो वह उसको भगवान् का ही गुण मानता है अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचारों, विकारों से मुक्त होता है। भक्त को तो भगवान ही प्रिय होते हैं अन्य कुछ नहीं।
संकलित – श्रीमद् भगवद् गीता।
साधक संजीवनी- श्रीस्वामी रामसुखदासजी।